नई दिल्ली. कोविड वैक्सीन लेने के बाद वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी (Antibody) विकसित होगी या नहीं, इस बात को लेकर लोगों के मन में भम्र है. वैक्सीन की प्रभावकारिता को पुख्ता करने के लिए लोग एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन इस तरह एंटीबॉडी जांच कराना क्या वास्तव में शरीर में कोविड वायरस के प्रति विकसित हुई एंटीबॉडी का पता लगाने में कारगर है. आईजीएम (IGM) और आईजीजी एंटीबॉडी (IGG Antibody) का क्या महत्व है? कोविड के बाद कौन सी एंटीबॉडी (Antibody After Covid) बनती है और वह कैसे पहचानी जाती है? अगर आप भी एंटीबॉडी जांच कराने के बारे में सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है.
जोधपुर स्थित आईसीएमआर, एनआईआईआरएनसीडी (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पलीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्यूनिकेबल डिसीज) के निदेशक और कम्यूनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. अरुण शर्मा एंटीबॉडी से लेकर इम्यूनिटी तक तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं.
सवाल – किसी भी तरह का वायरल संक्रमण होने और एंटीबॉडी के बीच में क्या संबंध है?
जवाब – जब कोई भी वायरस (Virus) मानव शरीर पर आक्रमण करता है तब शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम उसकी पहचान फॉरेन बॉडी के रूप में करता है और उससे लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. किसी भी वायरस का पहली बार हमला होने पर शरीर में वायरस के प्रति कारगर या असरदार एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाती है, ऐसी अवस्था में संक्रमण बहुत गंभीर होता है. जबकि दूसरी बार संक्रमण होने पर वह फॉरेन बॉडी या वायरस को तुरंत पहचान लेती हैं और वायरस के प्रति लड़ने के लिए अधिक बेहतर मात्रा में एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं. शरीर में संक्रमण का स्तर अधिक होने का मतलब यह भी है कि यह अधिक मात्रा में अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है. इसके लिए संक्रमण के डिसेमिनेशन रूट (वायरस के फैलने के रास्ते) होते हैं जैसे कोविड के डिसेमिनेशन का रूट रेस्पेरेटरी सिस्टम से है. खांसने से. छींकने से, तेज बोलने से वायरस हवा में आ जाता है और तेजी से लोगों को संक्रमित करने लगता है. इम्यूनिटी और वायरस में यही संबंध है कि वायरस नया होता है या जब म्यूटेडेड होता है तो उसको शरीर पहचान नहीं पाता या एंटीबॉडी नहीं होती है जैसे जैसे इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनने लगती है संक्रमण का खतरा कम होने लगता है.
सवाल – आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी जांच का कोविड संक्रमण में क्या महत्व है?

एंटीबॉडी टेस्ट कोविड का पता काफी तेजी से लगाता है. Image Credit : Pixabay
जवाब – कोविड में दो तरह से एंटीबॉडी जांच की जाती है या एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया दो चरण में होती है एक लघुकालीन या कम समय की और दूसरी दीर्घकालीन या अधिक समय की एंटीबॉडी. वायरस के शरीर पर हमला करने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया के तौर पर जो एंटीबॉडी बनती है वह आईजीएम एंटीबॉडी होती है और बाद में बनने वाली एंटीबॉडी आईजीजी कहलाती है. अधिक समय तक चलने वाली एंटीबॉडी आईजीजी कहलाएगी. संक्रमण के तुरंत बाद मिलने वाली एंटीबॉडी को आईजीएम कहा जाता है. ज्यादातर लोग वैक्सीन लेने के 21वें दिन पर एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं. एंटीबॉडी जांच में दोनों ही तरह की एंटीबॉडी होगी लेकिन आईजीजी एंटीबॉडी अधिक दिनों तक रहती है, जबकि आईजीएम एंटीबॉडी कम समय के लिए बनती है. वैक्सीन लगने या संक्रमण होने, दोनों ही स्थिति में हमें आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है. इसलिए शरीर में मजबूत एंटीबॉडी आईजीजी को माना जाता है.
सवाल – न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या है?
जवाब – एंटीबॉडी के काम करने का अलग सिद्धांत होता है. वायरस की भी सेल्स होती हैं. वायरस एक यूनिसेल्यूलर आर्गेनिज्म या एककोशकीय जीव होता है. इसके सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है और एंटीबॉडी रिसेप्टर पर जाकर चिपक जाती हैं. कोविड में वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अहम माना गया है, जिसे “एस” प्रोटीन भी कहा जाता है. संक्रमण या वैक्सीन के माध्यम से स्पाइक प्रोटीन के प्रति एंटीबॉडी बनती हैं और यह स्पाइक प्रोटीन पर जाकर उसे बाइंड कर देती हैं. इससे स्पाइक प्रोटीन का वायरस को जिंदा रखने क काम नहीं हो पाता या वह काम करना बंद कर देता है. इसे हम स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रालाइज या निष्क्रिय करना कहते हैं. वायरस को न्यूट्रलाइज करने से यह शरीर को अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है.
सवाल – वैक्सीन प्रभावकारिता का क्या सभी पर अलग असर पड़ता है, कुछ लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं देखी गई?
जवाब – अगर आपने वैक्सीन ले ली तब भी एंटीबॉडी नहीं बनी तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है. वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी टाइटल्स का स्तर कम आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत है. इसका जवाब जानने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि एंटीबॉडी क्यों नहीं बनी? क्या आपके शरीर में कोई जेनेटिक कंपोजिशन है या इससे संबंधित कुछ ऐसी दिक्कत है जो एंटीबॉडी को बनने से रोक रहे हैं. इसलिए अगर वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी तो पहले यह आपको इसकी वजह का पता लगाना होगा. ऐसा होने पर इम्यूनोलॉजिस्ट से संपर्क करने के बाद आपको पैथोलॉजिस्ट से पूरी जांच करानी चाहिए.
सवाल- कोविड में किस तरह की इम्यूनिटी की भूमिका अधिक है?
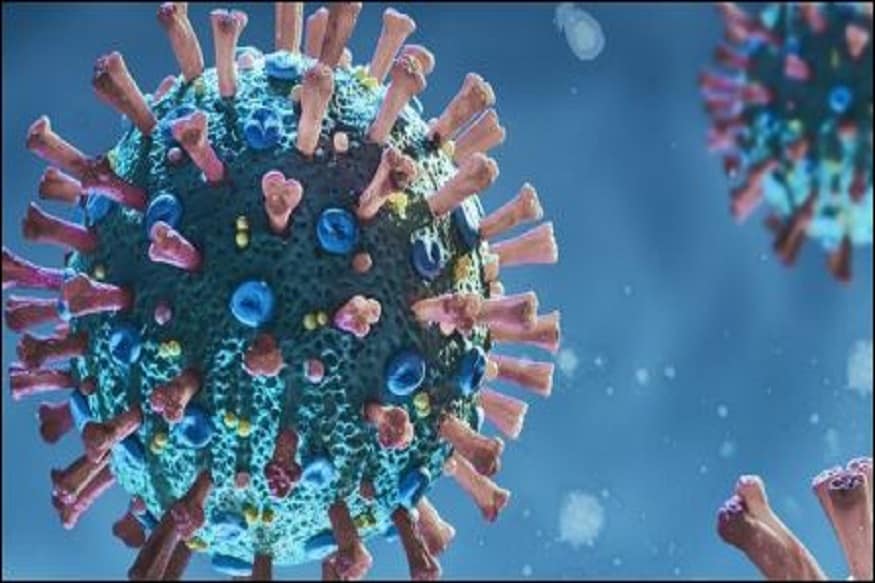
कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी अगर एंटीबॉडी नहीं बन रहीं तो टेस्ट कराने की जरूरत है.
जवाब – कोविड में हम शरीर में हृयुमोरल एंटीबॉडी देखते हैं. हृयुमोरल इम्यूनिटी को समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि टी सेल्स भी दो तरह की होती है. एक टी हेल्पर सेल्स होती है और दूसरी टी सेपरेशन सेल्स होती हैं. टी हेल्पर सेल्स वायरस को पहचाने का काम करती हैं. वायरस का हमला होने पर वह पहचान लेती हैं कि इस तरह के वायरस ने पहले भी कभी हमारे शरीर पर हमला किया था. वह वायरस को याद रखती हैं और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं. वायरस उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. वायरस को हमारी सेल्स पहचान लेती हैं यह उसको खत्म करने में सहायता करती है. टी सेपरेशन सेल्स का जबकि कुछ अलग तरह का बायोलॉजिकल काम होता है.
सवाल – इम्यून रेस्पांस क्या है, वायरस के म्यूटेडेड होने से इससे क्या संबंध है?
जवाब – वायरस की जो संरचना होती है या वायरस में जो प्रोटीन होते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन को पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है. जब वायरस म्यूटेडेड या जब वायरस में म्यूटेशन होता है तो वायरस अपने प्रोटीन की आकृति बदल लेता है. इसको ऐसे समझते हैं कि मान लें एक ताले के लिए हमने चाबी बनाई और बाद में यदि ताले में बदलाव हो गया तो बनाई गई चाबी ताले के किसी काम की नहीं होगी. वायरस ने अपने एंटीजन की संरचना बदल ली, अब वह नया एंटीजन हो गया. नया एंटीजन पुराने एंटीजन से कितना अलग है इस पर निर्भर करेगा कि एंटीबॉडी नए एंटीजन पर काम कर रही है या नहीं. अभी तक जितने भी वेरिएंट देखे गए हैं उन सभी पर वैक्सीन कारगर साबित हुई है. म्यूटेशन होना स्वाभाविक है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है. यदि म्यूटेशन पर एंटीबॉडी कारगर नहीं है तो हमें नई वैक्सीन लानी होगी.
सवाल – सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? इसका पता लगाने के लिए कौन सी जांच कराई जा सकती है और यह इम्यूनिटी कितने समय तक रहती है?
जवाब – इम्यूनिटी दो तरह की होती है एक हृयुमोरल इम्यूनिटी और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिनमें हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी का काम करती है. पोलियो, हेपेटाइटिस बी या कोविड संक्रमण में बीमारी से लड़ने की इम्युनिटी ही इन बीमारियों से लड़ती हैं लेकिन ट्युबरक्लोसिस या टीबी में एंटीबॉडी काम नहीं आती है टीबी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम आती है. इसका मतलब हुआ कि जो इम्यून सेल्स होती है वह इस बात की पहचान कर लेती हैं कि इस शरीर में अगली बार अगर टीबी अगर आएगा तो यह सेल्स जाकर बैक्टीरिया को क्षतिग्रस्त या खत्म कर देती हैं. इसमें टी सेल्स का अहम रोल होता है.
शरीर में दो तरह की सेल्स होती हैं एक बी सेल्स और दूसरी टी सेल्स. जो बी सेल्स होती हैं वह एंटीबॉडी बनाती हैं और टी सेल्स होती है वह सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं. टी सेल्स संक्रमण के कारक वायरस को खा (इंगल्फ) जाती हैं. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की भी हम जांच कर सकते हैं, इनके वायरस के प्रति रिएक्शन या प्रतिक्रिया होती है. टीबी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है इसकी जांच को मैनटॉक्स जांच कहा जाता है. इसमें हम स्किन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का एंटीजन डाल देते हैं और इसके बाद सेल्स की क्रिया प्रतिक्रिया देखते हैं, जिससे एंटीबॉडी का पता लग जाता है.
सवाल – कोविड टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी जांच कराना क्या सही है?
जवाब – व्यक्तिगत रूप से एंटीबॉडी जांच कराने में कोई बुराई नहीं है. किसी भी प्रमाणित या अधिकृत लैबोरेटरी से यह एंटीबॉडी जांच कराई जा सकती है लेकिन एक सरकारी व्यवस्था की तरह यदि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उन लोगों की एंटीबॉडी जांच भी की जाए तो यह संभव नही है, और इसका कोई फायदा भी नही है. कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडी टाइल्स से बनी एंटीबॉडी जांच की जाती है
सवाल –वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड संक्रमण होने की अहम वजह क्या हो सकती है?
जवाब – कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वह फिलहाल ब्लड या खून में बन रही हैं. वह एंटीबॉडी वायरस को तब ही मारेगी जब वह खून तक पहुंचेगा. वायरस ब्लड में कब पहुंचेगा? जब वह रेस्पेरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को पार कर लेता है क्योंकि कोविड का वायरस संक्रमित हवा के जरिए सबसे पहले नाक में पहुंचता है इसके बाद वह ट्रैकिया या श्वांस नली से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है. श्वांस नलिका में रहते हुए वायरस अपनी संख्या बढ़ा सकता है और यह लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी लगातार संक्रमित करता रहेगा इस संदर्भ में हम नेजल स्प्रे वैक्सीन को अधिक कारगर कह सकते हैं क्योंकि नेजल वैक्सीन नाक में म्यूकस मैंबरेन को प्रोटेक्ट कर देगी. जैसे हम पोलियो की ओरल ड्राप देते हैं, इससे पूरे गट या अमाश्य के ऊपर वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच बन जाता है. नाक से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाना जरूरी है.
सवाल – वैक्सीन संक्रमण के गंभीर खतरों को कम करने में कैसे कारगर हो सकती है?
जवाब – माइल्ड या हल्का कोविड संक्रमण होने का मतलब है कि वायरस हमारे नाक और गले में है. इस स्थिति में गले में दर्द खांसी होगी और हल्का सा बुखार होगा. अब यह वायरस जब फेपड़े की एल्बूलाई (जहां से फेफड़ों में खून पहुंचता है) में पहुंचेगा और जैसे ही यह ब्लड में प्रवेश करेगा वहां मौजूद एंटीबॉडी उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगीं यानि ब्लड के पास जाने के बाद वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाया. इसलिए वैक्सीन लेने के बाद गंभीर बीमारी नही होगी. अब अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं ली हुई और इस स्थिति में वायरस फेपड़े से ब्लड में पहुंचेगा तो ब्लड में वह तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है क्योंकि यहां उसको रोकने के लिए किसी तरह का रक्षा कवच नहीं होगा, फिर ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं.





